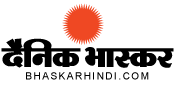- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- ईआरटी मॉडल : फ्लाईएश प्रदूषित भूमि...
Nagpur News: ईआरटी मॉडल : फ्लाईएश प्रदूषित भूमि को मिलेगा नया जीवन

- सीएसआईआर नीरी ने विकसित की तकनीक
- नागपुर के वैज्ञानिकों की टीम की उलब्धि
Nagpur News चंद्रकांत चावरे . सीएसआईआर-नीरी (वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) नागपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने पर्यावरण पुनरुद्धार की दिशा में क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने इको-रिजुवेनेशन टेक्नालॉजी (ईआरटी) विकसित की है। इस तकनीक की मदद से फ्लाई ऐश (राख) से बंजर हो चुकी या प्रदूषित हो चुकी भूमि को हरित व उपजाऊ भूमि बनाया जा रहा है। भूमि को पुनर्जीवित करने की इस प्रक्रिया की शुरुआत नागपुर से की गई है। अब यह तकनीक अन्य राज्यों में भी अपनाई जाने वाली है। सीएसआईआर-नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. लाल सिंह व उनकी ने पर्यावरण पुनरुद्धार की दिशा में लंबी अवधि तक प्रयोग किया है। इसके बाद इको रिजुवेनेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस तकनीक की मदद से फ्लाई ऐश से बर्बाद हो चुकी जमीन को हरित और उपजाऊ क्षेत्र में बदला जा रहा है। अब तक इस तकनीक से 60 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा चुका है।
भूमि का प्राकृतिक स्वरूप : ईआरटी तकनीक एक प्राकृतिक समाधान है। इसमें बायोरिमेडिएशन, फाइटो रिस्टोरेशन, जैविक खाद, बांस रोपण का समावेश है। स्थानीय लोगों की भागीदारी से प्रदूषित भूमि को फिर से उपजाऊ और हरा-भरा बनाया जाता है। यह तकनीक न केवल मिट्टी की सेहत को सुधारती है, बल्कि जैव विविधता को भी बढ़ावा देती है। इसमें फ्लाई ऐश युक्त जमीन पर विशेष रूप से चयनित बांस की विविध प्रजातियों का उपयोग करती है। बांस की गहरी जड़ें मिट्टी को स्थिर करने में मदद करती है। बांस में भारी धातुओं को अवशोषित करने और जैव विविधता को पुनः बहाल करने की शक्ति होती है। इस तकनीक से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, हरियाली लौटती है और प्रदूषित भूमि की बंद हो चुकी स्वाभाविक प्रक्रिया को नया जीवन मिलता है। इन पुनर्जीवित स्थलों पर अब स्थानीय वनस्पति, पक्षी, तितलियाँ, छोटे स्तनधारी और अन्य जीव-जंतु वापस लौट आए हैं। कभी बंजर और राख से भरे ये क्षेत्र अब हरे-भरे इको-सिस्टम में बदल गए हैं। यह बदलाव केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
मॉडल की देश भर में मांग : इस तकनीक का जन्म नागपुर स्थित सीएसआईआर-नीरी मुख्यालय में हुआ। डॉ. लाल सिंह और उनकी टीम ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर और कोराडी स्थित थर्मल पावर स्टेशनों के पास फ्लाई ऐश से प्रभावित ज़मीन को चिन्हित किया गया। ईआरटी तकनीक के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब यह मॉडल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। ईआरटी के तहत नागपुर के कोराडी, खापरखेड़ा व चंद्रपुर में 33 महिला बचत समूहों का गठन किया गया है। इनमें 660 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर भूमि पुनर्जीवन, पौधारोपण, खाद मिश्रण और स्थल रख-रखाव के कार्य में लगाया गया। हर समूह में 20 महिलाएं शामिल हैं। यह महिलाएं न केवल पर्यावरण सुधार में भागीदार बनीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मिली है।
2017 से अध्ययन व प्रयोग 2017 से दो साल तक नागपुर में कोराडी व खापरखेड़ा क्षेत्र में 10 हेक्टेयर भूमि पर प्रयोग किया गया। इसके चार साल में यह भूमि उपजाऊ, हरी-भरी बनी। कोराडी, खापरखेड़ा व चंद्रपुर में अब तक 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बांस का उपयोग कर हरित भूमि विकसित की गई है। बताया गया कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का करीब 29.3% (96.4 मिलियन हेक्टेयर) हिस्सा वर्तमान में बंजर या मरुस्थलीकरण की स्थिति में है। फ्लाई ऐश, थर्मल पावर प्लांट्स से निकलने वाला अत्यंत विषैला अपशिष्ट इस समस्या का बड़ा कारण है। इस तकनीक का उपयोग देश भर के अलग-अलग राज्यों में किया जाएगा।
प्रकृति हुई पुनर्जीवित : सीएसआईआर-नीरी द्वारा विकसित इको-रिजुवेनेशन टेक्नोलॉजी की मदद से देश के कई फ्लाई ऐश डंप साइट्स को पुनर्जीवित कर वहां फिर से जैव विविधता लौटाई गई है। हमने जब मिट्टी को उपचार दिया, तो प्रकृति ने स्वयं को पुनर्जीवित कर लिया। हमने बंजर ज़मीनों को हरा-भरा किया और साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाया। यही इकोलॉजिकल जस्टिस है। -डॉ. लाल सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर-नीरी, नागपुर
रोजगार की नई राह : ईआरटी न सिर्फ पर्यावरण के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि इससे स्थानीय लोगाें को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। बांस की खेती से जुड़े काम, जैसे पौधारोपण, सिंचाई, देखभाल, कटाई, और बांस उत्पादों का निर्माण के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों को ईआरटी से जोड़ा गया है। सीएसआईआर-नीरी द्वारा चयनित बांस की प्रजातियांे की मांग तेजी से बढ़ने वाली हैं। यह प्रजातियां न केवल भूमि का उपचार करती हैं, बल्कि निर्माण कार्य, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट और कागज उद्योग में भी उपयोगी हैं। इससे बांस आधारित स्टार्ट-अप्स के लिए नये अवसर के द्वार खुलेंगे। े अनेक राज्यों की सरकारें, पर्यावरण विभाग और पावर कंपनियां अपने क्षेत्र में लागू करने में रुचि दिखा रही है।
Created On : 4 July 2025 11:16 AM IST